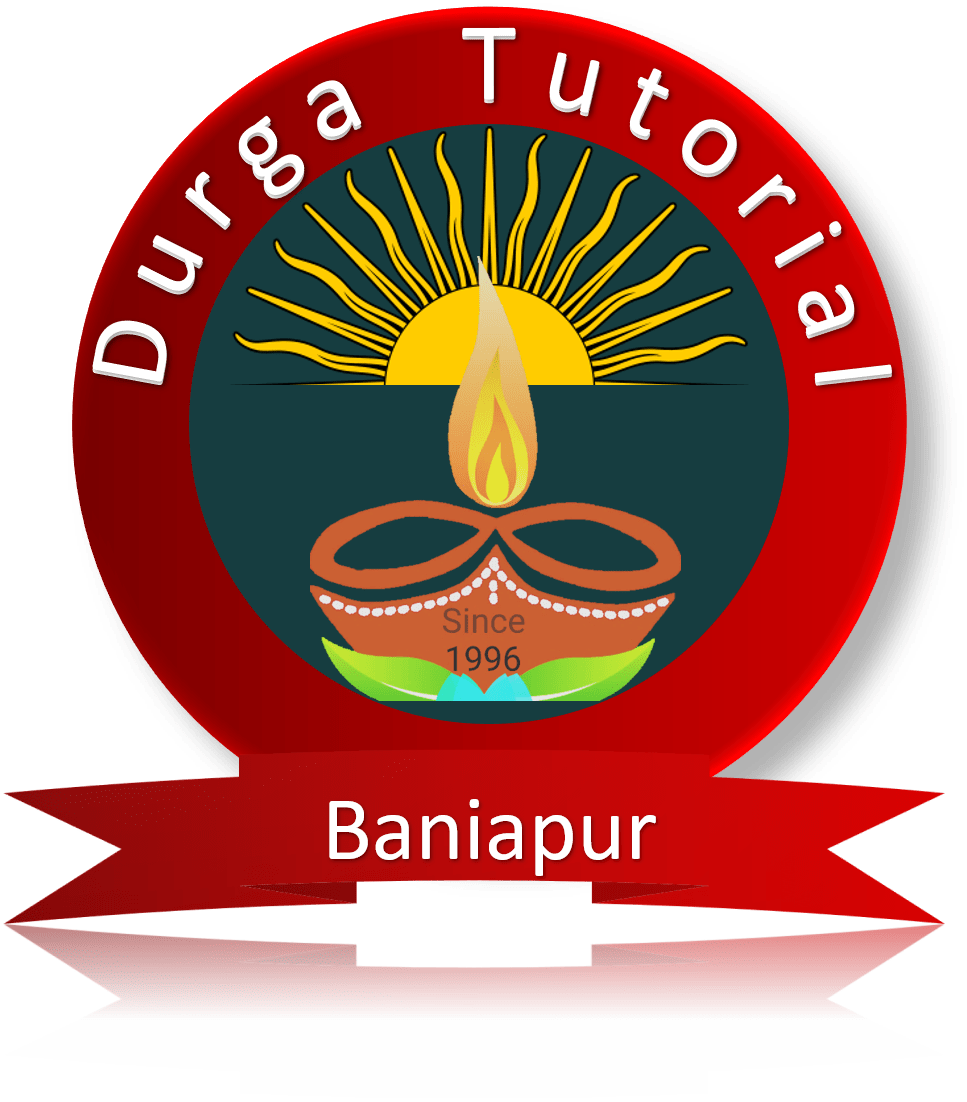कारक परिभाषा-संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थात्, क्रिया के होने या करने में जो (संज्ञा या सर्वनाम) सहायक हो, उसे कारक कहते हैं।
जैसे-राम ने रावण को मारा वाण से ऋषि के लिए।
दूर घर से देवसरिता की तटी में हे प्रिय।
इस पद में ‘राम ने’, ‘रावण को’, ‘वाण से’, ‘ऋषि के लिए’, ‘घर से दूर’, ‘देवसरिता की’, ‘तटी में’, ‘हे प्रिय’- संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध ‘मारना’ क्रिया के साथ सूचित होता है ।
कारक के भेद हिन्दी में आठ कारक हैं। इनके नाम, विभक्तियाँ और लक्षण निम्नांकित हैं:-
| कारक | विभक्ति |
| कर्ता | ओ, ने |
| कर्म | ओ, को |
| करण | से |
| संप्रदान | को, के, लिए |
| अपादान | से |
| संबंध | का,के,की |
| अधिकरण | में, पर |
| संबोधन | हे,हो, अरे, अजी, अहो |
कर्ताकारक- जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया संपादित हो, उसे कर्ताकारक कहते हैं।
जैसे- लड़का पढ़ता है ।
नौकर ने दरवाजा खोला ।
चिट्ठी भेजी जाएगी।
इन वाक्यों में ‘लड़का’, ‘नौकर’ और ‘चिट्ठी’ कर्ताकारक हैं, क्योंकि उनका संबंध क्रमशः ‘पढ़ना’, ‘खोलना’ और ‘भेजना’ क्रियाओं के साथ है।
कर्मकारक जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे सूचित करने वाली संज्ञा के रूप को कर्मकारक कहते हैं।
जैसे- लड़का किताब पढ़ता।
राम ने रावण को मारा ।
इन वाक्यों में ‘किताब’ एवं ‘रावण’ कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल इन्हीं दोनों शब्दों पर पड़ता है। इसलिए, इसका रूप होगा- ‘किताब को’ तथा ‘रावण को’ ।
करणकारक-करणकारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं, जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है ।
जैसे—सिपाही चोर को रस्सी से बाँधता है ।
लड़का कलम से लिखता है ।
मनुष्य आँखों से देखते हैं ।
इन वाक्यों में ‘रस्सी से’, ‘कलम से’ और ‘आँखों से’ में क्रिया के साधन का बोध होता है; अर्थात् संज्ञा और क्रिया के बीच कर्म का संबंध जाहिर हो रहा है।
संप्रदानकारक – जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है, उसकी वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदानकारक कहते हैं।
जैसे—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया।
शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं।
लड़का पढ़ने को गया है।
इन वाक्यों में ‘को’ के प्रयोग से यह पता चलता है कि किस वस्तु के लिए क्रिया संपन्न की जा रही है।
अपादानकारक- अपादानकारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं, जिससे क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है। अर्थात् जिससे किसी वस्तु के एक-दूसरे से अलग होने के भाव का बोध हो।
जैसे— पेड़ से पत्ता गिरा ।
गंगा हिमालय से निकलती है।
इन वाक्यों में ‘से’ का प्रयोग एक-दूसरे से अलग होने के भाव को प्रदर्शित करता है।
संबंधकारक- संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है, उस रूप को संबंधकारक कहते हैं।
जैसे—यह राजा का महल है।
वह किताब राम की है।
इन वाक्यों में ‘महल’ का संबंध राजा से तथा ‘किताब’ का संबंध राम से निर्दिष्ट किया गया है। अतः एक-दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखलाया गया है।
अधिकरणकारक-संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता हैं, अधिकरणकारक कहलाता है।
जैसे— सिंह वन में रहता है।
बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है।
इन वाक्यों में ‘वन में’ और ‘पेड़ पर’ क्रमश: ‘रहना’ और ‘चढ़ना’ क्रिया के आधार का बोधक है, इसलिए अधिकरणकारक है।
संबोधनकारक-संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है, उसे संबोधनकारक कहते हैं ।
जैसे- हे राम ! तुम कहाँ हो ।
हे भगवान ! तुम उनकी रक्षा करना ।
यहाँ ‘हे राम’ और ‘हे भगवान’ दोनों ही संबोधन के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।